पंजू: Panju (This Hindi story is about a family servant who became necessity of every family member. As time passed, requirement and love for the servant changed.)
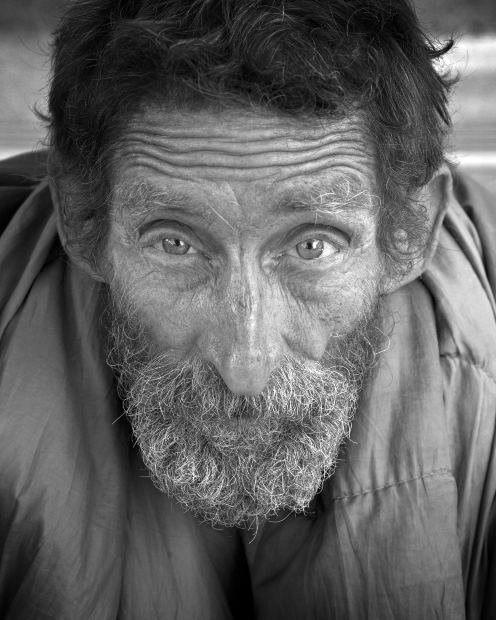
Hindi Story – Panju
Photo credit: BBoomerinDenial from morguefile.com
(Note: Image does not illustrate or has any resemblance with characters depicted in the story)
ईश्वर ही जाने, पंजू उसका असली नाम था अथवा यथा-कथित प्रचलित! और हां, उसके माता-पिता कौन थे, और कहां के रहने वाले थे, इसकी जानकारी तो ठीक ठीक शायद ही किसी को रही हो। कम से कम मुझको तो नहीं है। मेरा ज्ञान तो उसके बारे में न के बराबर है। हां, जितना मुझे अपनी धर्मपत्नी से मालूम हुआ, वो शाहणी के साथ उसके मायके से ही आया था। मेरी सास ने शायद कभी अपनी बेटी को पंजू के बारे में बताया होगा, कि पंजू शाहणी के मायके में बर्तन-पोचा करने वाली एक ग़रीब औरत का बच्चा था जो माँ की उंगली पकड़ कर उनके घर आया करता था, कि अचानक एक दिन पंजू की माँ उस यतीम को मालकिन के हवाले छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई।
भला वक़्त था। उसी घर में बचा-खुचा खाकर पंजू बड़ा होने लगा। घर का छोटा-मोटा काम कर दिया करता था और ज़्यादा समय शाहणी के साथ बचपन में खेला करता था। इससे दोनों में ऐसा लगाव हो गया कि उसे शाहणी के साथ ही भाई की जगह डोली के साथ भेज दिया गया, क्योंकि शाहणी का कोई भाई नहीं था। पंजाब में रिवाज के अनुसार दुल्हन का भाई डोली के साथ बहन के ससुराल आता है, और दो-एक रोज़ रुक कर बहन को वापिस लिवा ले जाता है। बहन के ससुराल में भाई की ख़ूब ख़ातिर की जाती है। खाने को भरपेट मिठाईयाँ, और वापसी पर ख़ास तौर पर तैयार की हुई पोशाक, जो वो अपने साथ अपने घर ले आता है। इसलिये किसी को तन्ज़िया उसकी औकात जताने के लिये कहा जाता है कि, ’क्या तू डोली के साथ आया है?’ परन्तु पंजू डोली के साथ ऐसा आया कि फिर लौट कर नहीं गया। एक नौकर की क्या औकात! उसे तो सब कुछ वही करना होता जो वो शाहणी के मायके में किया करता था।
पंजू से मेरी मुलाकात पहली बार तब हुई जब मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। मेरे विचार में उन दिनों वो लगभग 45-50 का रहा होगा। ठिगना कद, भरा हुआ बेडौल शरीर, दबी हुई ठोड़ी, फूले गाल, घुटा हुआ सिर – जिसपर कनपटियों के पास बेतरतीब उगे हुए चन्द बाल, बड़े बड़े कान और एक मोटी सी नाक। भद्दे, मोटे मोटे होंठ और शरीर झुर्रियों से भरा, मगर मज़बूत। अच्छे हड्ड-काठ, बड़े बड़े मज़बूत हाथ और ढलकी हुईं मांसपेशियाँ। वो मानव की अपेक्षा बन-मानुष अधिक लगता था। अपनी ढलकी हुईं छातियों के कारण मुझे वो कोई विधवा स्त्री लगा जो झाड़ू बर्तन करने के लिये लगाई गई हो, जैसे आम तौर पर शादी ब्याह पर रख ली जाती हैं। वो एक मैली कुचैली लुंगी लपेटे, प्राय: खुले शरीर रहने का आदी था। एक लाल सा परना कभी कन्धों पर और कभी सिर पर डाले, वो हर कमरे में – क्या मर्दाना, क्या ज़नाना – बेधड़क घुस जाता था जैसे मुगलों के समय ऱव्वाजासराह हुआ करते थे जिनसे बेग़मात और शाही ख़ानदान की स्त्रियाँ तक परदा करना अनावश्यक समझती थीं।
सेठ नानकचंद के घर में पंजू को भी ऐसा प्राणी माना जाता था जिस से बहू बेटियाँ कोई पर्दा वर्दा नहीं करती थीं। सास तथा बहुओं, बेटियों के गहने कपड़े, यहां तक कि उस समय प्रचलित सौन्दर्य प्रसाधन – कंघी, शीशा, सिंदूर, बिंदी, अंजन, मंजन, दातुन, अंग्रेज़ी साबुन तथा ख़ुशबूदार तेल और इत्र फुलेल – प्राय: सभी वस्तुओं का अता-पता केवल पंजू को ही रहता। रसोईघर का तो वो मानो एकमात्र शासक था। घर में क्या बना है तथा बनाना है, क्या पड़ा है और दुकान से क्या लाना है, यह सब उसकी ज़िम्मेदारी थी। दुकान पर खाना गया कि नहीं, बैठक में हुक्का तैयार रखना वगैरह वगैरह, सब उसकी दिनचर्या में शामिल था।
सेठ नानकचंद दुकान से आते और जूता उतारते ही पुकार उठते, “पंजू!” और पंजू सब काम धाम छोड़ हवा में जैसे उड़ता हुआ पानी का गिलास लेकर हाज़िर हो जाता। लुंगी, पानी, परना, सेठ को थमाते हुए, आगे-पीछे फिरता रहता और घर के दैनिक समाचार – कौन आया, कौन गया – सब ब्योरा देता। सेठ को तो यह भी ज्ञात नहीं होता था कि पत्नी घर पर है अथवा कहीं बाहर गई है। और सच तो यह था कि शाहणी को अपनी हमजोली सहेलियों से हंसी-ठठ्ठे से कम ही फ़ुर्सत मिलती थी। वो अधिकतर सहेलियों के साथ माता के जागरण तथा कथा कीर्तन, गुरूद्वारे-मंदिर में अधिक ही रुचि रखती थी और देर सवेर ही घर लौटती। कई बार तो ऐसा भी होता कि अपनी सहेलियों के साथ कई कई दिन के लिये तीर्थ यात्रा पर निकल जाती।
सेठ नानकचंद का मकान मेरे ससुराल से लगता हुआ था। दोनों मकानों के आंगन को विभाजित करने वाली दीवार न जाने कब की गिर चुकी थी और किसी को भूले से भी उसको उठाने का विचार कभी नहीं आया। यूं समझ लो कि दोनों घरों के प्रेम-प्यार से ऐसा लगता था, जैसे एक ही परिवार हो।
पंजू मेरी सास को ’सेठानीजी’ कहकर पुकारता था। सुबह सुबह मैं अभी बिस्तर से उठा भी नहीं था कि पहली बार मेरे कान में पंजू की भौंडी (बेसुरी) आवाज़ पड़ी,”सेठाणीजी, मैं टुक्कस दे सारे भांडे कट्ठे कर दित्ते ने। तुलसी नूं कैणा गुरद्वारे छड्ड आवे।”
उन दिनों शादी-ब्याह के लिये बर्तन, दरी, ड्रम, हवन कुंड तथा मुकुट, और दूसरा ज़रूरी सामान, गुरूद्वारे-मंदिर का, तथा पंचायती हुआ करता था जो ज़रूरत के मुताबिक मंगवा लिया जाता। इसके साथ ही साथ छत से आवाज़ आई,”पंजू, मेरी जूंआँ आली कंघी ते दे जा।” फिर तो जैसे तूफ़ान ही आ गया। “पंजू, मेरा तौलिया, पेटीकोट दे जा”। पंजू का सबको एक ही जवाब होता, “आया जी।…” इतने में एक मर्दाना आवाज़ आई, “भई नाश्ता लगाओ ना! दुकान को देर हो रही है!” पंजू ने झट जवाब दिया, “शा जी, नाश्ता ते मेज़ ते रखया है। हुणे हाज़र होया।”
मेरी उत्सुक्ता बढ़ गई कि आख़िर यह पंजू है क्या बला! अभी अभी नहाकर निकली श्रीमतीजी से मालूम हुआ कि वो घर का नौकर है। मैंने हंस कर कहा, “नौकर न हुआ, अलादीन का जिन्न हो गया जो सबकी जी हुज़ूरी कर रहा है!”
उसको जानने की मेरी उत्सुक्ता और भी बढ़ गई जब खाने पर उसकी बाबत मेरी सास ने बताया कि, “’भागवंती’ को तो यहां तक भी होश नहीं कि उसके गहने कितने हैं और कहां पड़े हैं। यह सब कुछ सम्हालना पंजू का ही काम है। रसोइया तो वो एक नम्बर का है। अगर शादी-ब्याह का मौका न हो तो सौ पचास का खाना तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पर ही बना लेता है। मुर्गा, बटेर, बकरे का गोश्त बनाने में तो वो माहिर था। और मर्दों में तो इसलिये भी उसकी ख़ूब चलती थी।”
मेरे दादा-ससुर महीने-पंद्रह दिन में जब गांव से आते, बच्चों के लिये साथ ही साथ किसी कुल्फ़ीवाले तथा चाट-पकौड़ी या गोल-गप्पे वाली रेहड़ी लेते आते और दोनों परिवारों के बच्चे और औरतें जी भर कर खाते पीते। दुकान पर सूचना भेज दी जाती कि लालाजी गांव से आये हुए हैं। शाम को बोतल का प्रबन्ध होना चाहिये। पंजू गोश्त तैयार कर लेता था। देर तक खाना-पीना, हंसी मज़ाक चलता रहता और अगली बार के लिये सब अपनी अपनी फ़र्माईश लालाजी को कर देते। ऐसे मौकों पर पंजू का ’मुजरा’ ना हो, यह मानने वाली बात नहीं थी। जहां चार औरतों की महफ़िल जमी, पंजू ज़रूर मौजूद होता और हिजड़ों वाले अंदाज़ में फब्तियाँ कसता जिसका कोई बुरा नहीं मानता था।
आज इतने समय बाद मुझे पंजू के किरदार को लेखिनीबद्ध करने का विचार क्यों आया, इसकी भी अपनी एक कहानी है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बंटवारे के साथ साथ दिलो दिमाग़ तथा धन धाम, सभी बिखर गये। परन्तु सेठ नानकचंद और मेरे ससुर साहब के प्रेम में अन्तर नहीं आया। दोनों ने मिलकर घर का सामान तीन चार गड्डों पर दो नौकरों के साथ पंजू की निगरानी में हिन्दुस्तान रवाना कर दिया और ख़ुद हवाई जहाज़ द्वारा सपरिवार दिल्ली पहुँच गये। ईश्वर की दया से सामान के साथ पंजू भी यहां पहुँच गया। दोनों ने कस्टोडियन के द्वारा अलॉट किये हुए मकान तो ले लिये लेकिन अब वे एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। अपने अपने तौर पर दोनों ने रोज़गार तो बनाये, परन्तु सेठ नानकचंद का भाग्य कुछ ज़्यादा तेज़ निकला। लड़के कारोबार में ख़ूब कामयाब हुए और प्राय: सभी लड़कों की तथा दो लड़कियों की शादी धूमधाम से हुई।
मेरे ससुर साहब का ताल्लुक तो ख़ैर बना रहा, लेकिन मेरी मुलाकात कभी शादी-ब्याह या दुख-तकलीफ़ में ही हुआ करती। शाहणी और सेठ नानकचंद मुझे बहुत प्यार करते थे और जब भी मुलाकात होती, बहुत मान सम्मान देते। जब भी कभी उनके यहां जाता, पंजू को ख़ुश-ओ-ख़ुर्रम पाता। उसके अधिकार क्षेत्र में अभी तक कोई विशेष अन्तर नहीं महसूस किया। घर में अब दो नौकर और भी थे। परन्तु पंजू की ज़रूरत सब को थी।
बातों बातों में एक दिन श्रीमतीजी ने मुझे बताया कि पंजू अब वो पंजू नहीं रहा। उसके भी दिल्ली आकर पर निकल आये हैं। मैं यह सुनकर अवाक् रह गया कि इस उम्र में पर कैसे निकल आये, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य वृद्धावस्था में तो कन्धों पर अपना ही बोझ बर्दाश्त नहीं करता, पर लगाकर क्या करेगा – क्योंकि उड़ने के लिये तो परों की अपेक्षा कन्धों का बलिष्ठ होना अत्यावश्यक है। ख़ैर, मैंने सुनी अनसुनी कर दी क्योंकि मेरी रुचि अब पंजू अथवा सेठ नानक चंद जी के परिवार में बहुत कम थी।
उस समय तो मैंने श्रीमतीजी की बात में रुचि नहीं ली, परन्तु समय समय पर पता चलता रहा कि सेठ के छोटे लड़के ने – जाने क्या नाम है उसका – एक बार पंजू पर अपनी बीवी का हार चुराने का आरोप लगाया जिसकी चर्चा बाद में नहीं हुई। शायद हार मिल गया होगा।
परन्तु अब की बार आरोप बहुत गन्दा था। छोटी बहू ने छेड़खानी की शिकायत की और पंजू की जम कर पिटाई की गई।
अब क्योंकि मुझे सेठ नानकचंद के लड़कों के नाम याद नहीं हैं, इसलिये मैं सुविधा के लिये उन्हें बड़े, मंझले, और छोटे ही कहूंगा। ख़ैर, छोटे अब अपनी बीवी को लेकर मुंबई चला गया है। शाहणी का स्वर्गवास हो चुका है। लड़कियाँ अपने अपने घरों में सुखी हैं। अब पंजू के अतिरिक्त दो नौकर और पांच व्यक्ति परिवार में रहते हैं। दो भाई – बड़े और मंझले, उनकी बीवियाँ, और एक लड़का।
बड़े को थोड़ी सी पीने पिलाने की आदत है। नानकचंद का अब इतना रुतबा तो नहीं है लेकिन लड़का चोरी छिपे ही पीता है। सेठ नानकचंद को न जाने क्यों चीखने चिल्लाने की आदत सी हो गई है। बात बात पर बच्चों के काम-काज में मीन मेख निकालते रहते हैं। लगता है, सभी उनसे दुखी हैं।
मैं जब शाहणी की मातमपुर्सी को गया था तो पता चला, सेठजी नर्सिंग होम में हैं। मैं सहानुभूति वश एक दिन सेठ नानकचंद को देखने नर्सिंग होम जा पहुँचा। कोने के कमरे में पलंग पर पड़ा एक बूढ़ा पथराई हुई सी आँखों से टुकर टुकर निहार रहा था, जैसे होशोहवास खो चुका हो। मेरे सामने होते ही उसकी आँखों में चमक सी आ गई। मैं हैरान हो गया जब छूटते ही सेठ ने मेरा नाम लेकर तपाक से मेरा स्वागत किया। आँखों से झर झर आँसू बह रहे थे। मेरे दिलासा देने पर रुदन रुका नहीं, और तीव्र हो गया, मानो मुद्दत से रुके हुए आँसुओं की बाढ़ आ गई हो। या जैसे सावन भादों के बादल फटने के लिये अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। बहुत कुरेदने पर भी सिवाय ठंडी सांसों के, परिवार के विरुद्ध उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि बेटों के रूखे बर्ताव का दुख उनके चेहरे पर साफ़ दिखाई दे रहा था। और तो और किसी प्रकार की दुनियादारी निबाहने तक की परवाह किसी को नहीं थी, जिसकी इत्तलाह मुझे समय समय पर मिलती रही। आज वही वीरान आँखें हर आते जाते व्यक्ति को टुकर टुकर निहारती हुई देखने में आईं।
गुरूद्वारा शीशगंज के बाहर, खम्बे के साथ पीठ लगाये पंजू बैठा था। उसने तो शायद मुझे नहीं पहचाना। और मैंने भी उसकी आँखों से ओझल होने की कोशिश की। जी में तो आया कि लिवाकर अपने घर ले जाऊँ और यथाशक्ति देखभाल करूं, मगर मुझे यह मानने में थोड़ा संकोच और लज्जा हो रही है कि दो परिवारों के पिछले घनिष्ठ सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए उस लावारिस बूढ़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। और नई पीढ़ी के ख़ुदगर्ज़ रवैये पर खीझता रहा कि बड़े बूढ़ों की भावनाओं का रत्ती भर विचार न करते हुए उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं।
यही व्यवहार कल जब उनके साथ होगा तो सम्भवत: वे सहन नहीं कर पायेंगे।
समाप्त
लेखक :- जगदीश लूथरा ‘नक्काद’
